स्व और पर कल्याण का साधन… दान!
– अंतर्मुखी मुनि पूज्य सागर महारज
स्व और पर कल्याण का साधन रहा दान आज हमारे जीवन में अहम संतुष्टि का साधन बन·र रह गया है। जिस दान को देने से देने और लेने वाले दोनों का ही हित होता हो वह दान बड़े पैमाने पर होकर भी संसार में वह सुख , शांति और समृद्धि नहीं ला पा रहा जो उसका मूलगुण है। इसी कारण यह सोचने का विषय है कि क्या हम आज दान करते हैं..?
भारतीय परंपरा में दान का अत्यधिकमहत्व है। हमारी मान्यताओं के अनुसार दान, स्व और पर कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इससे विचारों की शुद्धि के साथ मन भी विशुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। दान का अर्थ है जो आपका है या आपके पास है उससे मोह को कम करना या उसे किसी पात्र व्यक्ति को देना। दान देने से मनुष्य का शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक विकास होता है। संसार और मोक्ष के सभी सुख व सुवूसन दान से ही प्राप्त होते हैं। वर्तमान में आपके पास जो सम्मान, यश, समृद्धि व ख्याति है वह दान का ही प्रभाव है।
दान देने से हमारा कल्याण होता है यह समझकर दान देना चाहिए तभी दान का फल प्राप्त होता है। दूसरों का भला ·र रहे हैं यह सोचकर दिए गए दान का फल नहीं मिलता है क्योंकि उसमें अहम भाव का समावेश हो जाता है। दान देते समय भावों का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यकहै। दान देने से प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव जाग्रत होता है और यही भाव वर्तमान में हमारे विश्व, देश, समाज और परिवार की एकजुटता के लिए सबसे आवश्य· है। इसी की कमी के चलते तो अराजकता, असंतोष, वैमनस्य और हिंसा का वातावरण पैसलता जा रहा है।
कहा गया है…
आहार औषधियो रप्यु ·रणावासयोश्च दानेन।
वैय्यावृत्यं बु्रवते चतुरात्मत्वेन चतुस्त्रा:।।
उपरोक्त श्लोकका तात्पर्य है कि आहार, औषध, अभय और ज्ञान के भेद से वैय्यावृत्ति चार प्रकार की है। यही चार दान हैं। स्व व पर का उपकार करने केलिए अपनी वस्तु या धन का त्याग करना ही दान है। पात्र और दाता का उपकार हो इस बुद्धि से, रत्नत्रय ( आदर्श आचरण) से युक्त जीव के लिए अपने धन का त्याग करना दान ही है।
कहने का मतलब है कि दान चार प्रकार के होते हैं। आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान (शिक्षा)। इसके अलावा करूणा दान का जिक्र भी शास्त्रों में मिलता है। यह वह दान है जो हम करूणा भाव से करते हैं। किसी की शारीरिक, मानसिकऔर आर्थिकविक्षिप्तता या असमर्थता को देखजो करुणा भाव उत्पन्न होता है उसी के वशीभूत होकर किया गया दान करूणा दान कहलाता है।
आज हमारे चारों ओर आपसी ईष्र्या, गरीबी, भूखमरी, महामारियाँ, अशिक्षा, आपसी बैर भाव अत्यधिक बढ़ गया है। इसी से उपजी समस्याएँ दिन प्रतिदिन अपने पैर पसार रही हैं। इन सबका कारण है दान की परंपरा का लुप्त होना या सही मायने में दान न देना। प्राचीन काल में दान आमजन की चर्या में शामिल था। किसी के घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता था, घर पर आने वाले भिक्षार्थी को हर कोई अपनी-अपनी क्षमतानुसार दान देता था। आज दान या तो लोग देते नहीं, यदि दे भी देते हैं तो लोभ के वशीभूत होकर, जिसमें भी अहम भाव समाहित रहता है और यह दान की परिभाषा से परे है। कोई, वैससा भी दान करता हो अपने नाम और यश की कामना से ही करता है। दान का मूल ही है बिना स्वहित का भावना से अपनी किसी भी वस्तु, धन, संपदा का त्याग करना। भाव परहित का नहीं होना चाहिए। जब भावनाएँ ही विकृत होंगी तो दान का प्रभाव भी वह नहीं होगा जो होना चाहिए।
शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी कुल आय का एक चौथाई हिस्सा दान ·रना चाहिए। यही नहीं किसी-किसी ग्रंथ में तो आधी कमाई दान करने तक की बात कही गई है। जिसमें यह भी कहा गया है कि व्यक्ति अपने परिजन, कुटुम्ब और नौकर आदि के सहयोगार्थ भी दान करे। दान का अर्थ त्याग है और दान देने से हम विनयवान होते हैं। विनयवान व्यक्ति ही लौककि-पारलौककि सफलता अर्जित कर सकता है।
वास्तव में दान करने से मनुष्य मन को सुवूसन प्राप्त होता है और व्यक्ति दसों इंद्रियों के माध्यम से शुभकर्म को ग्रहण करता है। दान ही व्यक्ति को विचारों की शुद्धता, सुंदर व स्वस्थ्य शरीर के साथ मानसिक और भावनात्मक शुद्धता भी प्रदान करता है।
प्राचीन ग्रंथों में दान को लेकर कई कथाएँ हैं। कर्ण को तो दानवीर की उपाधि ही दी गई है क्योंकि वह दान देते समय यह नहीं सोचता था कि अगर में यह वस्तु दान कर दूँगा तो मेरा क्या होगा। आज हम दान करते हैं पर उसका जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है या अब हमारे लिए उसका महत्व नहीं रहा हो। अगर धन भी दान ·रते हैं तो केवल तब जब उससे हमें सम्मान या कोई लाभ प्राप्त हो रहा हो। इतिहास गवाह है कि नि:स्वार्थ भाव से दान देने वालों को हमेशा अच्छा प्रतिफल ही प्राप्त हुआ है। कई गाथाएँ दान के परिणामों की व्याख्या करते हैं। महान् विभूतियों ने अपने पास स्व के लिए बची एक रोटी को भी दान किया है और वह भी मुस्कुराते हुए। अगर आज हम मजबूरन कहीं कोई चंदा दे देते हैं तो सोचते हैं दान कर दिया पर वह वास्तविक दान नहीं है।
अतिफलदायी दान को देने वाले यानि कि दाता में कुछ गुणों का होना अनिवार्य है। दाता के मूल सात गुण कहे गए हैं। भक्ति, विनय, विद्वान, संतोष, क्षमा, उत्साह, सत्व और द्रव्य। इन गुणों का धारक ही सही मायने में दाता है। जो व्यक्ति इन गुणों का धनी होगा वह जब भी दान करेगा निर्लिप्त और नि:स्वार्थ भाव से ही करेगा तभी दान सही दाता द्वारा पात्र को प्राप्त हो सही फल देगा।
दान जितने विशुद्ध मन वाला व्यक्ति देगा और जितने विशुद्ध मन वाला व्यक्ति उसे ग्रहण करेगा उसका प्रतिफल भी उतना ही विशुद्ध होगा। यहाँ विशुद्ध का अर्थ चारित्रिक और मानसिक विशुद्धि से है। काले धन का दान काला ही प्रभाव देगा। गाड़ी ईमानदारी से ·माए धन का दान उतना ही शुद्ध फलदायी होगा। भारतीय परंपरा चारित्रिक विशुद्धि को सर्वाधिक महत्व देती है और इसीलिए दान भी उसी विशुद्धि के साथ देना चाहिए क्योंकि दान के प्रतिफल से ज्ञानशक्ति बढ़ती है। व्यक्ति पुण्यार्जन कर सांसारिक सुख भी प्राप्त करता है और अगले जन्म को भी संवारता है। दान देने से अच्छे कुल में जन्म बंध, तीर्थंकर बंध, सम्मान, संपूर्ण ज्ञान आदि का फल मिलता है। जो इतना फलदायी हो यदि वही देते समय हम विशुद्धि का ध्यान नहीं रखेंगे तो अच्छे परिणामों की चेष्टा ·रना भी व्यर्थ ही है।
अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर हम आज अपने देश को, समाज को और परिवार को उन्नति व विकास की नई बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं तो दान की ओर प्रवृत्त होना होगा क्योंकि यह वह साधन है जो हमें गरीबी, भूखमरी, महामारी, अराजकता, आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसी विकट समस्याओं से भी निजात दिला स·ता है।
निर्लिप्त और नि:स्वार्थ भाव से दान करें… और अमूल्य चारित्रि· समृद्धिशाली जीवन प्राप्त करें।

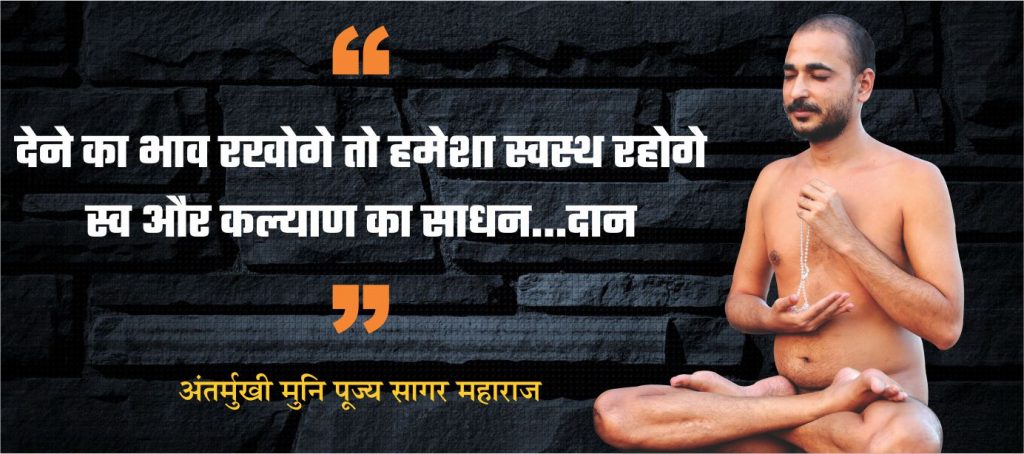
Give a Reply